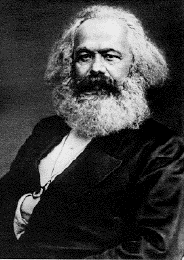चार-पांच दिन पहले, जब विमलेश त्रिपाठी के स्टेटस पर एक कवितानुमा रचना पढ़ी, उस पर टिप्पणी की और उसे शेयर भी किया, तब से ही कई तरह की बातें दिमाग़ की 'दांय' करने में लगी हैं. उस रचना का लब्बोलुबाव तो इतना भर था-- एक ने 'क' से लिखा 'कविता', दूसरे ने 'क' से लिखा 'कहानी' और तीसरे ने 'कुछ' भी न लिखा, और पुरस्कार उस तीसरे व्यक्ति को ही मिल गया. इसमें ऐसा क्या था जिससे मेरे दिमाग़ की दांय होनी चाहिए थी. मित्र, अमित्र, शत्रु सब एकमत हो कर कहेंगे, 'कुछ भी नहीं.' तो फिर?
'क' से 'कई' भी होता है, यानि कई बातें सिर उठाने लगीं. पहली तो यह कि वह रचना 'कविता' कही जा सकती भी है या नहीं? 'क' से बनता है 'कथ्य'. तो यदि वह 'कविता' है, तो उसमें कोई 'कथ्य' भी है या नहीं? 'क' से बनता है 'क्या', तो क्या 'कविता' और 'कहानी' लिख देने भर से इस रचना का 'कथ्य' निर्मित हो गया? या वह निर्मित हुआ तीसरे के 'कुछ न' लिखने से? या फिर 'कुछ न लिखने वाले' के पुरस्कृत हो जाने से? क्या वास्तव में ऐसा होता है /हो सकता है? यदि हां, तो भी क्या यह किसी क़ायदे की रचना का उपयुक्त कथ्य बन सकता है?
अच्छी रचनाओं को पीछे धकिया कर, बुरी ( या उतनी अच्छी नहीं) रचनाएं तात्कालिक रूप से यदा-कदा आगे आ जाएं और कम समर्थ रचनाकार अधिक समर्थ रचनाकारों से आगे निकल जाएं, दौड में; यह भी संभव है. हो भी चुका होगा कई बार. पर इस सबकी पड़ताल 'कभी' बाद में 'क्योंकि' इस समय, प्रमुख मुद्दा एकांतिक रूप से यह हो भी नहीं सकता.
कविता की मृत्यु की घोषणाएं इतनी बार हो चुकी हैं कि इनकी गिनती रख पाना भी संभव नहीं. पर इन तमाम घोषणाओं के बावजूद कविता न केवल ज़िंदा है, बल्कि उसकी सेहत भी पूरी तरह से ठीक है. अभी तीन दिन पहले ही बाबुषा की बहुत बढ़िया कविता पढ़ने को मिली :"वसीयत." पिछले सप्ताह लीना मल्होत्रा की "प्रतिलिपि" में छपी तीन कविताएं पढ़ीं. प्रेमचंद गांधी की कविता 'भाषा की बारादरी' भी इसी बीच आई. हरीश करमचन्दाणी की कविताएं भी. आवेश तिवारी की श्वेताम्बरा श्रृंखला की कविताओं के अलावा दूसरी कविताएं, अंजू शर्मा की कविता जिस पर तो लगभग घमासान ही मच गया था. अरुण देव और अपर्णा मनोज की भी विशेष ध्यानाकृष्ट करने वाली दो-दो कविताएं. तो बीस दिन के भीतर इतनी सारी अच्छी कविताओं का फेसबुक पर आ जाना एक अच्छा संकेत है. ये सिर्फ़ उदहारण हैं. कथ्य और शिल्प जहां एकमेक हो गए हैं. कथ्यविहीन कविताएं भी आ रही हैं, शब्दों के मनमाने प्रयोग वाली कविताएं भी. दो-तीन मित्र लोग मिलकर किसी कवि को 'जोड़-तोड़' से दूर रहने वाला घोषित कर देते हैं, और किसी को 'सबसे कम जादुई', और यह 'अहो रूपम, अहो ध्वनि' का खेल चलता है; तीन-चार मित्र मिलकर किन्हीं दो मित्रों को 'कविता के सबसे अधिक संजीदा आलोचक' घोषित कर देते हैं. और ध्यान देने की बात यह है कि जो कुछ भी इस घेरे के बाहर हो रहा है, वह उल्लेखनीय नहीं है इनकी नज़र में. कहीं कोई पुरस्कार/ सम्मान घोषित हो गया तो " कितनी कविताएं, कितने सम्मान" (!) जैसा उच्छ्वास निकलता है. अरे भाई, कवि हो तो किसी कवि के सम्मान पा जाने पर ऐसी टिप्पणी करने की क्या जरूरत है? और सम्मानों से ही परहेज़ करते हो या उन्हें स्वस्थ / सार्थक रचनाशीलता के लिए घातक मानते हो, तो सभी सम्मानितों /पुरस्कृतों को एक ही नज़र से देखो. या फिर खुलकर यह कहो कि फलां कवि को ग़लत आधारों पर पुरस्कृत/ सम्मानित किया गया है. तर्कसम्मत विश्लेषण कर सको तो 'सोने पर सुहागा.' पर दुर्भाग्य से यह सब हो नहीं रहा.
मैंने पिछली बार, अपने ब्लॉग 'सोची-समझी' पर, 'क' से कुमारेन्द्र पारसनाथ सिंह की दो कविताएं दी थीं. ये कविताएं 1974 में, हमने 'क्यों' में छापी थीं. यों उस अंक में उनकी आठ कविताएं छपी थीं. ये दोनों कविताएं उस वक़्त बेहद सराही गई थीं. 'कथ्य' की दृष्टि से देखें तो इस देश में अभी तक भी ऐसा कुछ नहीं घटित हो गया है, सामाजिक-राजनैतिक तौर पर, कि इन कविताओं की प्रासंगिकता कम/ खत्म हो गई हो. यह मानने के भी कोई कारण नहीं दिखते कि कुमारेन्द्र पारस नाथ सिंह के कृतित्व से परिचित लोग फेसबुक पर सक्रिय नहीं हैं. इसके एक दम उलट, यहां सक्रिय लोगों में सर्वाधिक कवि-टिप्पणीकार वे ही हैं जो भौगोलिक रूप से भी उस इलाके से / आसपास से आते हैं जो कुमारेंद्र की रचना भूमि/ कर्म भूमि था. मैं यह सब क्यों लिख रहा हूं? सिर्फ़ यह बात सार्वजानिक करने के लिए कि किसी भी रचना के संभाव्य प्रभाव का अनुमान लगा पाने में मैं पहली बार चूक गया. मुझे इन कविताओं को साझा करते वक़्त यह लगा था कि बहुत सारे कवि, संजीदा पाठक, और टिप्पणीकार इन कविताओं से नए सिरे से रू-ब-रू होने पर न केवल प्रसन्नता ज़ाहिर करेंगे, बल्कि इनकी समकालीन सन्दर्भों में प्रासंगिकता को रेखांकित करने का प्रयत्न भी करेंगे. अपनी विरासत से नए लोगों का परिचय भी वरना कैसे होगा? ऐसा हुआ नहीं. मुझे क्यों बुरा लगना चाहिए? कुमारेन्द्र अब हैं नहीं हमारे बीच, तो वह तो अच्छा/ बुरा लगने की ज़द से बहुत दूर जा चुके हैं. हां, फिर भी मुझे बुरा लगा. इसलिए कि मैं फेसबुक पर सक्रिय ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो कुमारेन्द्र का जब-तब उल्लेख भी करते रहे हैं अपने आलोचनात्मक लेखन में, और दो-चार दिन में कहीं 'लाइक' करके या एकाध वाक्य की टिप्पणी करके कुछ लोगों से अपना जुड़ाव भी व्यक्त करते रहते हैं. 'गंभीर कविता' की अनदेखी, और 'न-कविता' की प्रशस्ति -ये दोनों ही अपराध हैं, ख़ासकर उनके लिए जो कविता से अपनी प्रतिश्रुति घोषित करते रहते हैं. कुमारेन्द्र की इन कविताओं पर कुल 6 टिप्पणियां ( जिनमें से चार ने कविता की पंक्तियाँ उद्धृत भर कर दी थीं) आईं. एक, आशुतोष कुमार की तरफ़ से, आई जिसे पूरी टिप्पणी कहा जा सकता है :"इन कविताओं को फिर से पढ़ना महज़ कविता पढना नहीं है . उस गुजरे हुए दौर को पढ़ना भी है , जब अन्याय के खिलाफ शब्द हथियारों की तरह बरते जा रहे थे. और इस दौर में उस दौर को पढ़ना जब ' अन्याय ' और ' प्रतिरोध ' शब्द मात्र की तरह पढ़े जा रहे हों !"
कविता यदि हमारी मनःस्थितियों का चित्रण भर करती है तो वह कोई ख़ास तीर मार लेने वाला काम नहीं बन पाता. और फिर हम आलोचकों को कोसने लगते हैं; शिकायत करने लगते हैं कि उनकी वजह से "कविता की जान सांसत में" है, जबकि सच यह है कि अपनी जान को ही सांसत में महसूस कर रहे होते हैं. मज़ा देखिए, कि जान सांसत में है फिर भी हम कविता को अपना पर्याय बना लेते हैं.
यह फेसबुक की सीमा नहीं है, उसे बरतने वालों की, उस पर सक्रिय लोगों की विशिष्टता है या 'विशिष्ट' दिखने की चाहत है. क्या कविता में लोकतंत्र तब तक क़ायम हो सकता है जब तक कि कवियों और आलोचकों की लोकतंत्र में निष्ठा न हो? कवि को आलोचक तब तक ही अच्छे लगते रहें जब तक कि वे उस की प्रशंसा करते रहें? अपने अलावा अन्य कवियों की प्रशंसा में अपनी 'हेठी' क्यों माननी चाहिए? महिला कवि की प्रशंसा हो तो उसे 'लैंगिक पक्षपात' के रूप में ही क्यों देखा जाना चाहिए? कविता की अथवा किसी भी विधा में प्रस्तुत रचना की किसी वस्तुपरक कसौटी का तो मान किया ही जाना चाहिए. चार-छह पंक्तियों की कविताएं अपवाद स्वरुप ही टिकाऊ महत्त्व की हो सकती हैं, यह तो सहज बुद्धि से समझ में आ जाना चाहिए. डेढ़ पंक्ति के वाक्य में पूरी कविता यदि आ जाती है, एक साथ लिखने पर, तो उसके 'कालजयी' होने का भ्रम तो नहीं ही पाला जाना चाहिए.
फेसबुक सामाजिक अंतरजाल से जुड़ने का माध्यम यदि है, जैसा कि इसे कहा जाता है, तो क्या इसका निहितार्थ यह नहीं समझा जाना चाहिए कि इससे जुड़ने का मतलब है अधिक सामाजिक होना. सामाजिकता विकसित होने/ करने की एक अन्तर्निहित शर्त यह भी है कि व्यक्तिवादी आग्रहों को तिरोहित करने की प्रक्रिया से जुड़ लिया जाए. तभी कदाचित कविता का, और फिर कवि का, स्थान वैसा बन पाए जैसा हर कवि 'अपने लिए' चाहता है. मर्यादा बनाए रखकर की जाने वाली हर बहस इस दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगी, प्रत्येक के लिए. ऐसा मुझे लगता है. ज़रूरी नहीं कि आप इससे सहमत हों. विचार और चर्चा का फौरी प्रस्थान बिंदु तो यह बन ही सकता है.
'क' से 'कई' भी होता है, यानि कई बातें सिर उठाने लगीं. पहली तो यह कि वह रचना 'कविता' कही जा सकती भी है या नहीं? 'क' से बनता है 'कथ्य'. तो यदि वह 'कविता' है, तो उसमें कोई 'कथ्य' भी है या नहीं? 'क' से बनता है 'क्या', तो क्या 'कविता' और 'कहानी' लिख देने भर से इस रचना का 'कथ्य' निर्मित हो गया? या वह निर्मित हुआ तीसरे के 'कुछ न' लिखने से? या फिर 'कुछ न लिखने वाले' के पुरस्कृत हो जाने से? क्या वास्तव में ऐसा होता है /हो सकता है? यदि हां, तो भी क्या यह किसी क़ायदे की रचना का उपयुक्त कथ्य बन सकता है?
अच्छी रचनाओं को पीछे धकिया कर, बुरी ( या उतनी अच्छी नहीं) रचनाएं तात्कालिक रूप से यदा-कदा आगे आ जाएं और कम समर्थ रचनाकार अधिक समर्थ रचनाकारों से आगे निकल जाएं, दौड में; यह भी संभव है. हो भी चुका होगा कई बार. पर इस सबकी पड़ताल 'कभी' बाद में 'क्योंकि' इस समय, प्रमुख मुद्दा एकांतिक रूप से यह हो भी नहीं सकता.
कविता की मृत्यु की घोषणाएं इतनी बार हो चुकी हैं कि इनकी गिनती रख पाना भी संभव नहीं. पर इन तमाम घोषणाओं के बावजूद कविता न केवल ज़िंदा है, बल्कि उसकी सेहत भी पूरी तरह से ठीक है. अभी तीन दिन पहले ही बाबुषा की बहुत बढ़िया कविता पढ़ने को मिली :"वसीयत." पिछले सप्ताह लीना मल्होत्रा की "प्रतिलिपि" में छपी तीन कविताएं पढ़ीं. प्रेमचंद गांधी की कविता 'भाषा की बारादरी' भी इसी बीच आई. हरीश करमचन्दाणी की कविताएं भी. आवेश तिवारी की श्वेताम्बरा श्रृंखला की कविताओं के अलावा दूसरी कविताएं, अंजू शर्मा की कविता जिस पर तो लगभग घमासान ही मच गया था. अरुण देव और अपर्णा मनोज की भी विशेष ध्यानाकृष्ट करने वाली दो-दो कविताएं. तो बीस दिन के भीतर इतनी सारी अच्छी कविताओं का फेसबुक पर आ जाना एक अच्छा संकेत है. ये सिर्फ़ उदहारण हैं. कथ्य और शिल्प जहां एकमेक हो गए हैं. कथ्यविहीन कविताएं भी आ रही हैं, शब्दों के मनमाने प्रयोग वाली कविताएं भी. दो-तीन मित्र लोग मिलकर किसी कवि को 'जोड़-तोड़' से दूर रहने वाला घोषित कर देते हैं, और किसी को 'सबसे कम जादुई', और यह 'अहो रूपम, अहो ध्वनि' का खेल चलता है; तीन-चार मित्र मिलकर किन्हीं दो मित्रों को 'कविता के सबसे अधिक संजीदा आलोचक' घोषित कर देते हैं. और ध्यान देने की बात यह है कि जो कुछ भी इस घेरे के बाहर हो रहा है, वह उल्लेखनीय नहीं है इनकी नज़र में. कहीं कोई पुरस्कार/ सम्मान घोषित हो गया तो " कितनी कविताएं, कितने सम्मान" (!) जैसा उच्छ्वास निकलता है. अरे भाई, कवि हो तो किसी कवि के सम्मान पा जाने पर ऐसी टिप्पणी करने की क्या जरूरत है? और सम्मानों से ही परहेज़ करते हो या उन्हें स्वस्थ / सार्थक रचनाशीलता के लिए घातक मानते हो, तो सभी सम्मानितों /पुरस्कृतों को एक ही नज़र से देखो. या फिर खुलकर यह कहो कि फलां कवि को ग़लत आधारों पर पुरस्कृत/ सम्मानित किया गया है. तर्कसम्मत विश्लेषण कर सको तो 'सोने पर सुहागा.' पर दुर्भाग्य से यह सब हो नहीं रहा.
मैंने पिछली बार, अपने ब्लॉग 'सोची-समझी' पर, 'क' से कुमारेन्द्र पारसनाथ सिंह की दो कविताएं दी थीं. ये कविताएं 1974 में, हमने 'क्यों' में छापी थीं. यों उस अंक में उनकी आठ कविताएं छपी थीं. ये दोनों कविताएं उस वक़्त बेहद सराही गई थीं. 'कथ्य' की दृष्टि से देखें तो इस देश में अभी तक भी ऐसा कुछ नहीं घटित हो गया है, सामाजिक-राजनैतिक तौर पर, कि इन कविताओं की प्रासंगिकता कम/ खत्म हो गई हो. यह मानने के भी कोई कारण नहीं दिखते कि कुमारेन्द्र पारस नाथ सिंह के कृतित्व से परिचित लोग फेसबुक पर सक्रिय नहीं हैं. इसके एक दम उलट, यहां सक्रिय लोगों में सर्वाधिक कवि-टिप्पणीकार वे ही हैं जो भौगोलिक रूप से भी उस इलाके से / आसपास से आते हैं जो कुमारेंद्र की रचना भूमि/ कर्म भूमि था. मैं यह सब क्यों लिख रहा हूं? सिर्फ़ यह बात सार्वजानिक करने के लिए कि किसी भी रचना के संभाव्य प्रभाव का अनुमान लगा पाने में मैं पहली बार चूक गया. मुझे इन कविताओं को साझा करते वक़्त यह लगा था कि बहुत सारे कवि, संजीदा पाठक, और टिप्पणीकार इन कविताओं से नए सिरे से रू-ब-रू होने पर न केवल प्रसन्नता ज़ाहिर करेंगे, बल्कि इनकी समकालीन सन्दर्भों में प्रासंगिकता को रेखांकित करने का प्रयत्न भी करेंगे. अपनी विरासत से नए लोगों का परिचय भी वरना कैसे होगा? ऐसा हुआ नहीं. मुझे क्यों बुरा लगना चाहिए? कुमारेन्द्र अब हैं नहीं हमारे बीच, तो वह तो अच्छा/ बुरा लगने की ज़द से बहुत दूर जा चुके हैं. हां, फिर भी मुझे बुरा लगा. इसलिए कि मैं फेसबुक पर सक्रिय ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो कुमारेन्द्र का जब-तब उल्लेख भी करते रहे हैं अपने आलोचनात्मक लेखन में, और दो-चार दिन में कहीं 'लाइक' करके या एकाध वाक्य की टिप्पणी करके कुछ लोगों से अपना जुड़ाव भी व्यक्त करते रहते हैं. 'गंभीर कविता' की अनदेखी, और 'न-कविता' की प्रशस्ति -ये दोनों ही अपराध हैं, ख़ासकर उनके लिए जो कविता से अपनी प्रतिश्रुति घोषित करते रहते हैं. कुमारेन्द्र की इन कविताओं पर कुल 6 टिप्पणियां ( जिनमें से चार ने कविता की पंक्तियाँ उद्धृत भर कर दी थीं) आईं. एक, आशुतोष कुमार की तरफ़ से, आई जिसे पूरी टिप्पणी कहा जा सकता है :"इन कविताओं को फिर से पढ़ना महज़ कविता पढना नहीं है . उस गुजरे हुए दौर को पढ़ना भी है , जब अन्याय के खिलाफ शब्द हथियारों की तरह बरते जा रहे थे. और इस दौर में उस दौर को पढ़ना जब ' अन्याय ' और ' प्रतिरोध ' शब्द मात्र की तरह पढ़े जा रहे हों !"
कविता यदि हमारी मनःस्थितियों का चित्रण भर करती है तो वह कोई ख़ास तीर मार लेने वाला काम नहीं बन पाता. और फिर हम आलोचकों को कोसने लगते हैं; शिकायत करने लगते हैं कि उनकी वजह से "कविता की जान सांसत में" है, जबकि सच यह है कि अपनी जान को ही सांसत में महसूस कर रहे होते हैं. मज़ा देखिए, कि जान सांसत में है फिर भी हम कविता को अपना पर्याय बना लेते हैं.
यह फेसबुक की सीमा नहीं है, उसे बरतने वालों की, उस पर सक्रिय लोगों की विशिष्टता है या 'विशिष्ट' दिखने की चाहत है. क्या कविता में लोकतंत्र तब तक क़ायम हो सकता है जब तक कि कवियों और आलोचकों की लोकतंत्र में निष्ठा न हो? कवि को आलोचक तब तक ही अच्छे लगते रहें जब तक कि वे उस की प्रशंसा करते रहें? अपने अलावा अन्य कवियों की प्रशंसा में अपनी 'हेठी' क्यों माननी चाहिए? महिला कवि की प्रशंसा हो तो उसे 'लैंगिक पक्षपात' के रूप में ही क्यों देखा जाना चाहिए? कविता की अथवा किसी भी विधा में प्रस्तुत रचना की किसी वस्तुपरक कसौटी का तो मान किया ही जाना चाहिए. चार-छह पंक्तियों की कविताएं अपवाद स्वरुप ही टिकाऊ महत्त्व की हो सकती हैं, यह तो सहज बुद्धि से समझ में आ जाना चाहिए. डेढ़ पंक्ति के वाक्य में पूरी कविता यदि आ जाती है, एक साथ लिखने पर, तो उसके 'कालजयी' होने का भ्रम तो नहीं ही पाला जाना चाहिए.
फेसबुक सामाजिक अंतरजाल से जुड़ने का माध्यम यदि है, जैसा कि इसे कहा जाता है, तो क्या इसका निहितार्थ यह नहीं समझा जाना चाहिए कि इससे जुड़ने का मतलब है अधिक सामाजिक होना. सामाजिकता विकसित होने/ करने की एक अन्तर्निहित शर्त यह भी है कि व्यक्तिवादी आग्रहों को तिरोहित करने की प्रक्रिया से जुड़ लिया जाए. तभी कदाचित कविता का, और फिर कवि का, स्थान वैसा बन पाए जैसा हर कवि 'अपने लिए' चाहता है. मर्यादा बनाए रखकर की जाने वाली हर बहस इस दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगी, प्रत्येक के लिए. ऐसा मुझे लगता है. ज़रूरी नहीं कि आप इससे सहमत हों. विचार और चर्चा का फौरी प्रस्थान बिंदु तो यह बन ही सकता है.